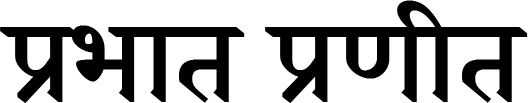अरुण कमल
अरुण कमल की कविता ‘प्रलय’ का पाठ :
पहले से विकसित होती सभ्यताओं ने हमें कितने घाव दिये हैं, हमें किन-किन जगहों पर बेधा है और कितनी तरह से अक्षम, पराजित साबित किया है, क्या इसका कोई प्रामाणिक हिसाब है हमारे पास? क्या इसकी विवेचना हेतु कोई प्रयास भी कहीं हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि जिस दिन ऐसा कोई प्रयास प्रारंभ होगा उसी दिन यह रोज सृजित होती सभ्यताओं का अश्लील नृत्य भी रुक जायेगा और स्वाभाविक है इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा. लेकिन जब भी धरती और आकाश की स्थापित सीमाओं के उल्लंघन का साहस रखने वाली कोई संवेदनशील आत्मा इसकी तह को उघाड़ना चाहेगी, उसका एक प्रकटीकरण अरुण कमल की कविता प्रलय के रूप में भी होगा.
एक चील के मुँह में साँप
साँप के मुँह में मेंढ़क
मेंढक के मुँह में कीट
उड़ी जा रही चील नीले स्वच्छ गगन में
नीचे पानी केवल पानी पानी पानी
कहीं नहीं धरती न रेत न हिमालय
प्रलय प्रलय प्रलय
यातना, याचना, संघर्ष और अंधकार के बीच के हर तड़प का लेखा-जोखा है ‘प्रलय’. फिर सहज ही है कि कवि शहर में आती लाशों की गिनती करने की भी कोशिश करते हैं और यह भी देख पाते हैं कि मृत्यु का अनुष्ठान करने वाला सबसे गरीब ही होता है. सभ्य होने, बनाने या तमाम तरह की सत्ता हथियाने की होड़ मनुष्य को रोज अकेला करती जा रही है, यह तो सभी जानते हैं लेकिन कवि इसके निष्कर्ष को खंगालते हैं और पाते हैं कि इसकी नियति किस हद तक संकीर्ण है- तभी तो हर व्यक्ति एक राष्ट्र होगा, उसका अपना ध्वज होगा और हर जाति का अपना कवि भी होगा. क्या हम इस निष्कर्ष के बहुत करीब हैं?
यह अब कोई आश्चर्य भी प्रतीत नहीं होता जब ‘गांधी’ झाड़ू का नाम भर बनकर रह जाएं और हमें रोज निर्देशित करने वाली हिदायत देती सूची में यह भी हो कि ‘ऐसे रहो जैसे पूरा शरीर जला हो’. यह प्रश्न तो कहीं खो चुका है कि गाँधी को क्यों मिटा दिया गया, (वैसे यह प्रश्न करने की अहर्ता प्राप्ति का लोभ कइयों के मन में रहा है और चूंकि ज्यादातर इसमें असफल रहे हैं इसलिए यह समय भी असफल ही रहा है, यह सबकी हार है, यही इस युग की पराजय है जिसे हर वर्ष बड़े जोश से जश्न के रूप में याद किया जाता है), प्रश्न तो अब यह है कि गाँधी के अवशेषों की पोटली अब भी दृष्टिगोचर क्यों है, और चूंकि यह भी अनुत्तरित है इसलिए आज और आने वाले कल की तमाम तबाही के दोषी भी यही हैं, हर रास्ता इनके पास से हो कर ही गुजरता है और यहीं समाप्त भी हो जाता है. हर इंच को बस में करते दीर्घ प्रतीक्षित स्वप्न से ठीक विपरीत ध्रुव, अब यथार्थ है. ‘पतित पावन सीता राम’ नेपथ्य में हैं, मुख्य भूमि पर तो लंकेश रावण का कब्जा है.
गाँधी तो अब एक झाड़ू का नाम है
नोट रुपइये पर आश्रम है धाम है
कब की सूख चुकी साबरमती
सब पोपले हो चुके हैं
झड़ चुके हैं उनके दाँत
(दाँतों का पहला काम काटना था आदिम युग में)
पर उनसे मुझे कुछ नहीं कहना
मैं तो पूछ रहा हूँ उनसे जो हर बार खाने के बाद
जतन से धोते हैं अपने दाँत अगले भोजन की प्रत्याशा में
तभी किसी ने पर्चा थमाया
पूरी हिदायत है पक्की सूची
क्या करना क्या न करना
क्या खाना क्या न खाना
सोते वक्त सिर किधर
क्या पहनना कितना पहनना
ऐसे रहो जैसे पूरा शरीर जला हो
और यह सिलसिला अनवरत है, सर्वत्र है. हमारी आश्चर्यजनक विडम्बनाओं ने हमें कुछ इस कदर जकड़ रखा है कि हमारे चेतन, अचेतन का वजूद अब एक कठपुतली से ज्यादा कुछ भी नहीं है. सबकुछ यन्त्रवत है और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है. मनुष्य होने का अहसास फिर किंचित चुभन भर का मोहताज रह जाता है और जो सर्वसुलभ है वह तो हम कभी थे ही नहीं. अब हम बस अदृश्य बनकर रह गए हैं जिसे सिर्फ देखना भर है, संजय की तरह. अदृश्य हो कर मौजूद रहना और समय, असमय जीवित हो जाना ही इक्कसवीं सदी की बड़ी उपलब्धि है, जीत है. आजकल इसी प्रपंच को व्यवस्था के नाम से सुशोभित किया जाता है. कवि कहते हैं-
खून होगा
एक मूली के नाम पर
खून होगा किसी के सामने खाँसने पर
जम्हाई देशद्रोह रोना देशद्रोह
खून होगा एक निवाले पर
डूबेगा देश गंगा के चुल्लू भर
माँ मेरी गंगा
बहुत दोष है मुझमें पर संतोष है यही कि
हम तुम्हारे पड़ोस में हैं
यही अपराध है माँ क्षमा करो
कि हमने तुम्हारा स्पर्श किया पैर से
अरुण कमल की एक कविता है ‘इच्छा’ जिसमें वे कहते हैं -‘इतना भरा हो संसार कि जब मैं उठूं तो चींटी भर जगह भी खाली न हो’, उस कविता में उनकी दृष्टि, उनकी बेचैनी बार-बार हमें जमीन की उन परतों तक ले जाती है जिन्हें हम अस्वाभाविक रूप से रोज भूल रहे हैं. वे परतें ही हमारे पैरों को टिकने को मजबूर करती हैं. लेकिन इस कविता में वे न सिर्फ हमारे अंतः, हमारे अस्तित्व को झकझोरते हैं बल्कि सारी सृष्टि, तमाम सभ्यताओं की कहानी, चंद शब्दों में निरूपित करते हुए अंत की घोषणा भी करते हैं. जब वे कहते हैं कि ‘पूरा देश वध-स्थल की ओर जा रहा है’ तो फिर इसके बाद शेष बचता ही क्या है! सिवाय उनके ही कहे इस निष्कर्ष के कि ‘मुर्दों के टीलों पर शिलालेख अमर’. यह कविता दस्तावेज है मनुष्य जाति के भूत और प्राप्त वर्तमान का, उसकी सीमाओं और तड़प का, हवस का, विध्वंस का, अनंत काल तक जारी रहने वाले क्षय का, पराजय का.
[अरुण कमल की यह कविता ‘प्रलय’ उनके संग्रह ‘योगफल’ में प्रकाशित है.]