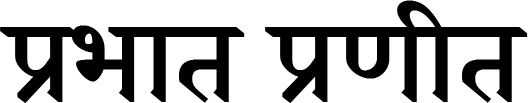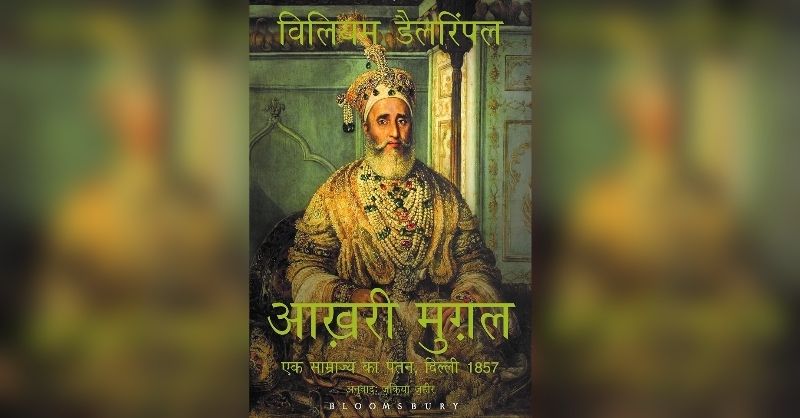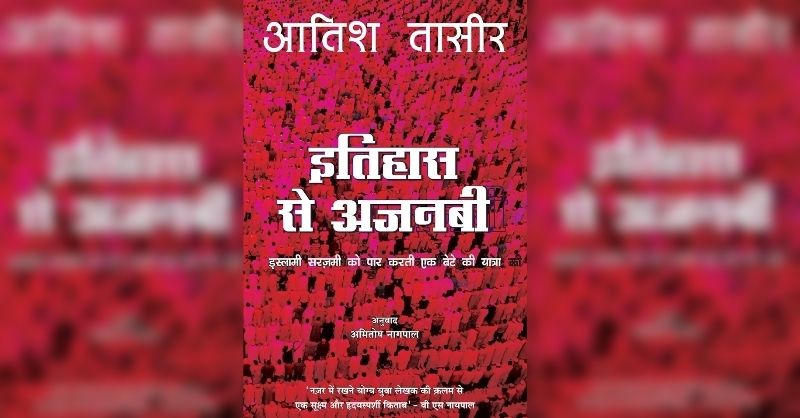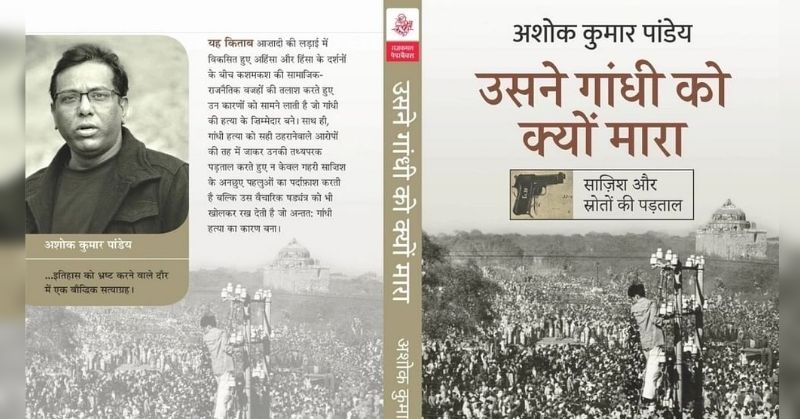फ़िल्म समीक्षा ::
देश, राष्ट्र, मुल्क की परिभाषा क्या होनी चाहिए इस बारे में कभी ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन जब भी जितना भी सोचा, इसकी किताबी परिभाषा से ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाया. मुल्क फिल्म में आरती मोहम्मद के चरित्र को निभा रही तापसी पन्नू जब कोर्ट में बोलती है कि “मुल्क कागज पर नक्शों की लकीरों से नहीं बंटता बल्कि मुल्क बंटता है दिमाग में, जाति में, धर्म में, नस्ल में, हम और वो में” तो विभाजन की इस व्याख्या से ही मुल्क की सही परिभाषा भी बनती दिखी. मुल्क जितना कागज पर बनता, बंटता है उससे ज्यादा हमारा जमीर उसे बनाता और बांटता है. चाहो तो धनश्याम और रिजवान मिलकर एक मुल्क है पर न चाहो तो धनश्याम और श्याम भी एक मुल्क नहीं है, रिजवान और इरफ़ान भी एक मुल्क नहीं है. तो टूट या जोड़ बाहर नहीं हमारे भीतर है, इतना तो यह फिल्म जरुर समझा गई और इस तरह अनुभव सिन्हा इस फिल्म को बनाने के अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहे हैं.
निम्नतम नाटकीयता के बावजूद अच्छी फिल्म बन सकती है और आपके जेहन को खोल सकती है यह बात इस फिल्म से साबित होती है. कैमरे का एंगल, पूरा फिल्मांकन कैमरामैन की आँखों से न हो कर इस फिल्म में आपकी हाथों और आँखों से होती प्रतीत होती है. कई बार तो लगता है जैसे आप कैमरा अपनी हाथों में ले कर चल रहे हैं. कैमरा जितना कहानी के साथ चलती है उतना आपके भीतर भी चलती रहती है. यह फिल्म जो फिल्म नहीं लगती है, यह कहानी जो कहानी नहीं लगती है और ऐसा होने में जितना योगदान अनुभव सिन्हा का है उससे ज्यादा योगदान पिछले कुछ वर्षों में हर तरफ, हर जगह दहक रहे गर्म हवा का है. फिल्म के दृश्य मुझे, मेरे अन्तः को उतना ही झुलसा रही थी जितना हर तरफ बह रही गर्म हवा मुझे रोज झुलसाती है.
ऐसा लगता है जैसे यह फ़िल्म सिर्फ अभी ही बननी थी, पहले शायद बन नहीं पाती और कुछ समय बाद सम्भवतः ज्यादा देर हो जाती. उचित समय कुछ चीजों के अस्तित्व से जुड़ा होता है, उसे जब होना चाहिए तब हो ही जाना चाहिए. प्रकृति स्वयं ही कई तरीकों से सुधार की कहानी बुनती रहती है, चेतावनी देने के तरीके ढूंढती रहती है. पता नहीं इस फ़िल्म के कथानक ने अनुभव सिन्हा को चुना या अनुभव सिन्हा ने इस फ़िल्म को पर इसका अभी घटित हो जाना, बन जाना सुकूनदेय है.
फिल्म की कहानी बंटवारे के वक्त मुसलमानों के लिए बनने वाले पाकिस्तान के बदले इस मुल्क को चुनने वाले एक आम मुसलमान परिवार के इर्द गिर्द घुमती है जिसके घर का एक सदस्य शाहिद धार्मिक उन्माद में बहक कर आतंकवादी बन जाता है. यह फिल्म एक आम मुसलमान के भटकाव को रेखांकित करने के साथ-साथ हमारे पूर्वाग्रह और सुनियोजित तरीके से हमारे मन में बसाई जा रही घातक धारणा के परत भी खोलती है और हमें आगाह भी करती है. एक ईमानदार मुस्लिम पुलिस अधिकारी दानिश जावेद के बहके मुसलमानों के प्रति अति आक्रामक व्यवहार उस चरित्र की कमी से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के भीतर पनप रहे दयनीय अन्तर्द्वन्द को रेखांकित करती है. मोराज अली मोहम्मद का चरित्र निभा रहे ऋषि कपूर जब सवाल करते हैं कि “कैसे साबित करूं अपना प्यार इस मुल्क के लिए” तो न सिर्फ उस चरित्र की विवशता पीड़ा देती है बल्कि इसी देश के नागरिक को यह उत्तर देने के लिए मजबूर किये जाने वाले सुनियोजित साजिश की भयावहता भी समझ में आती है. सच में कभी कोई मुझसे कहे कि तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो साबित करो, पता नहीं प्यार करते भी हो या नहीं, तो मैं क्या जबाब दूंगा, भला मैं कैसे साबित करूंगा ? कुछ सवाल तो कभी सवाल होते ही नहीं, वे तो दरअसल आग के गोले होते हैं जिसे हवा में उछाला ही इसलिए जाता है कि वह जहाँ गिरेगा आग ही लगायेगा. आज ऐसे सुनियोजित प्रश्नों को रोज ढूंढा जा रहा है, उसे रोज जोर से हवा में उछाला जा रहा है. मुल्क फिल्म ऐसे सवालों से बखूबी रू-ब-रू होती है.
इस फ़िल्म में जिहाद का सही अर्थ और आतंकवाद का सही मतलब दोनों को बतलाने की कोशिश अकादमिक नहीं व्यवहारिक है. किसी को डरा कर कोने में बैठाने की कोशिश, अस्पृश्यता, जातीय शोषण भी आतंकवाद ही है, याद करिये यह बात इससे पहले आपने किस न्यूज चैनल या सोशल मिडिया पर सुनी या पढ़ी थी, इस फिल्म में यह सुनते वक्त लगा जैसे फ़िल्मकार की नजर वहां बिल्कुल गई जहां जानी चाहिए और जहां अभी इस माहौल में सब अपनी नजर नहीं ले जा पा रहे.
फिल्म के कुछ दृश्य आपसे जुड़ से जाएंगे तो कुछ आवाज आपके भीतर रह जाएगी, आ जाएगी. जैसे शाहिद का विवश पिता जब बार-बार बोलता है कि “हमारा नाम बिलाल है, शाहिद आतंकवादी था, हम उसके बाप हैं” तो वह आवाज कई बार आपकी आवाज बन जाएगी, पात्र के सूखे आँखों का पानी आपकी आँखों में आ जायेगा. बचाव पक्ष के वकील द्वारा “गांधी को एक व्यक्ति ने मारा पूरी ब्राह्मण जाति ने नहीं” कहे जाने पर अहसास होता है कि किस कदर एक धर्म विशेष के प्रति हमारे मन में नाजायज घृणा भरी जा रही है. हमें अपने दादा के दादा का नाम याद नहीं और हमें सातवीं सदी में पहला अजान देने वाले बिलाल का नाम याद कराया जा रहा है, सदी पहले मिट चुके मुगलों की गलियों में हमें भटकाया जा रहा है, व्हाट्सएप्प यूनिवर्सिटी से हमारे दिमाग में जहरीला कूड़ा भरा जा रहा है. ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी और एक आम मुसलमान की दाढ़ी में फर्क करने की हमारी क्षमता इस हद तक खत्म की जा रही है कि हम इंसान बच ही न पाये और यह समाज, यह मुल्क जो है वह कुछ और बन जाये.
यह फिल्म कई बार और बार-बार फिल्म स्क्रीन से ज्यादा आपको अपने चारो तरफ चल रही दिखाई देगी. मुसलमानों के ज्यादा बच्चे पैदा करने और उनकी अशिक्षा पर तंज कसने वाले सरकारी वकील का चरित्र निभा रहे आशुतोष राणा की बातों पर जिस तरह स्क्रीन पर कोर्ट रूम में बैठे लोग खिलखिलाते हैं ठीक उसी समय, ठीक वैसी ही हंसी मैं सिनेमा हॉल के दर्शक दीर्घा में अपने चारो तरफ भी सुनता हूँ. और जब यह सुनता हूँ तो महसूस होता है कि हम वाकई कुछ ही समय में कितना बंट गये हैं, कितना टूट गये हैं, एक इंसान के तौर पर भी और एक मुल्क के तौर पर भी. मन भारी हो जाता है, कुछ बिखर सा जाता है. अपने मुल्क के पराया हो जाने या हो रहे होने की जिस पीड़ा को घोषित और अघोषित बंटवारे के वक्त करोड़ों लोगों ने महसूस किया है और कर रहे हैं उसका ही कुछ अंश मैं भी महसूस करने लगता हूँ.
तापसी पन्नू, मनोज पाहवा, ऋषि कपूर, आशुतोष राणा लगभग सभी ने अपने चरित्र के साथ न्याय किया है, वैसे यह भी हो सकता है कि इस फिल्म को देखते वक्त कई बार इसे फिल्म नहीं समझ पाने और मान पाने की वजह से मैं कलाकारों के अभिनय का सटीक मूल्यांकन नहीं कर पाया होऊं.
इस फिल्म को जरुर देखिये, सम्भव हो तो अपने अपनों को भी दिखाइए, क्या पता किसे गर्म हवा ने अपने चपेट में ले लिया हो और उसका बदन भी जल्दी ही तपने वाला हो, यह फिल्म उनके लिए शायद दवा का काम कर जाए.
***